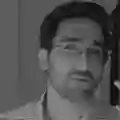न मंज़िलें थीं न कुछ दिल में था न सर में था
न मंज़िलें थीं न कुछ दिल में था न सर में था
'अजब नज़ारा-ए-ला-सम्तियत नज़र में था
इताब था किसी लम्हे का इक ज़माने पर
किसी को चैन न बाहर था और न घर में था
छुपा के ले गया दुनिया से अपने दिल के घाव
कि एक शख़्स बहुत ताक़ इस हुनर में था
किसी के लौटने की जब सदा सुनी तो खुला
कि मेरे साथ कोई और भी सफ़र में था
कभी मैं आब के तामीर-कर्दा क़स्र में हूँ
कभी हवा में बनाए हुए से घर में था
झिजक रहा था वो कहने से कोई बात ऐसी
मैं चुप खड़ा था कि सब कुछ मेरी नज़र में था
यही समझ के उसे ख़ुद सदा न दी मैंने
वो तेज़-गाम किसी दूर के सफ़र में था
कभी हूँ तेरी ख़मोशी के कटते साहिल पर
कभी मैं लौटती आवाज़ के भँवर में था
हमारी आँख में आ कर बना इक अश्क वो रंग
जो बर्ग-ए-सब्ज़ के अंदर न शाख़-ए-तर में था
कोई भी घर में समझता न था मेरे दुख सुख
एक अजनबी की तरह मैं ख़ुद अपने घर में था
अभी न बरसे थे 'बानी' घिरे हुए बादल
मैं उड़ती ख़ाक की मानिंद रहगुज़र में था
More by Rajinder Manchanda Bani
As you were reading Shayari by Rajinder Manchanda Bani
Similar Writers
our suggestion based on Rajinder Manchanda Bani
Similar Moods
As you were reading undefined Shayari